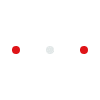कांग्रेस लंबे समय से नीति, नेतृत्व और रणनीति को लेकर भ्रम का शिकार रही है। नीति का मतलब है विचारधारा। कांग्रेस की विचारधारा क्या है यही आज स्पष्ट नहीं है। इस बार का उसका घोषणा पत्र कई पहलुओं में अतिवादी वामपंथियों का घोषणा पत्र लगता था। यह देश में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली तथा स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत की पार्टी के वैचारिक दिशाभ्रम का प्रमाण ही है।
नई दिल्ली: इसमें दो राय नहीं कि कांग्रेस गंभीर संकट से गुजर रही है। चुनावी दुर्दशा के बाद पार्टी कार्यसमिति की बैठक विचार मंथन के लिए बुलाई गई थी। किंतु इतनी बड़ी पराजय के कारणों और भविष्य के लिए रास्ते तय करने के लिए लंबी अवधि के ईमानदार और निर्भीक विचार मंथन की आवश्यकता है। करीब दो दर्जन नेताओं की कुछ घंटे की बैठक में यह संभव ही नहीं था। वहां से जो कुछ निकलकर आया उसमें अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे का प्रस्ताव सर्वप्रमुख बन गया।
पार्टी की ओर से पत्रकार वार्ता में बताया गया कि नेताओं ने उनको साफ कर दिया है कि अध्यक्ष के रुप में हमें आपकी जरुरत है। हम हार के कारणों पर विचार करेंगे लेकिन नफरत और विभाजन की राजनीति के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अंदर क्या हुआ इसकी मोटा-मोटी जानकारी ही मिल सकी है।
मसलन, इसमें राहुल गांधी ने कई नेताओं का नाम लेकर कहा कि उन्होंने पार्टी हित की जगह पुत्र हित को महत्व दिया। अपने बेटों को टिकट देने पर अड़ गए। जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां से गलत फीडबैक देने के कारण भी वे नाराज थे। इसमें दूसरों के लिए बोलने की जगह कम ही रही होगी। कई प्रदेश अध्यक्षों तथा प्रभारियों का इस्तीफा आना आरंभ हो गया है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलेगा।
2014 के आम चुनाव में पराजय के बाद भी कुछ राज्यों के अध्यक्षों ने अपना इस्तीफा भेजा था जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इस बार क्या होगा कहना कठिन है। खबर आ रही है कि राहुल गांधी को नेताओं ने मना लिया है कि वो अध्यक्ष पद न छोड़ें। तो देखते हैं क्या होता है। प्रश्न है कि क्या इस्तीफा से कांग्रेस के पुनर्जीवन का रास्ता निकल सकता है?
सही मायने में कांग्रेस के सामने राष्ट्रव्यापी दल के रुप में अस्तित्व का संकट है। लगातार दो चुनावों में दो अंकों तक सिमट जाना तथा लोकसभा में विपक्ष का दर्जा हासिल करने योग्य 10 प्रतिशत मत भी न पाना ऐसी स्थिति है जिसकी कल्पना कांग्रेसी नेताओं ने दुःस्वप्नों में भी नहीं की होगी।
वैसे भी इस बार कांग्रेस यह मानकर चल रही थी कि नरेन्द्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ पूरे देश में माहौल है तथा राफेल को लेकर उन पर भ्रष्टाचार का दाग हम लगाने में सफल हो चुके है, इसलिए पराजय निश्चित है। कांग्रेस को सभी विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा इतनी सीटें आने की उम्मीद थी जिससे सरकार गठन में उसकी निर्णायक भूमिका होगी।
इस उम्मीद में स्थिति यह हो गई कि राहुल गांधी अपने परिवार की परंपरागत सीट अमेठी से हार गए। अमेठी से हारना अपने-आपमें कांग्रेस के लिए सबसे बड़े दुर्दिन का द्योतक है। वे उस हालत में हारे जब सपा-बसपा ने वहां से उम्मीदवार नहीं उतारा था। अगर वे केरल के वायनाड नहीं गए होते तो लोकसभा से बाहर रहते। यह असाधारण आघात है। 1977 में इंदिरा गांधी की रायबरेली से राजनाराण जी के हाथों पराजय जैसा इसका महत्व भले न हो लेकिन इसके लिए दूसरा कोई उदाहरण दिया भी नहीं जा सकता।
हालांकि अभी भी भाजपा के बाद सबसे ज्यादा मत उसके खाते ही है। किंतु यह ऐसा नहीं है जिसमें संतोष का कोई भी पहलू हो। पिछले चुनाव से उसकी आठ सीटें तथा 0.1 प्रतिशत मत अगर बढ़ा है उसमें तमिलनाडु और केरल का योगदान है। तमिलनाडु में द्रमुक की कृपा से वह आठ सीटें तथा केरल में 15 सीटें जीत गई। यानी 52 में से 23 सीटें इसी राज्य से हैं।
केरल में कांग्रेस की विजय सबरीमाला आंदोलन के कारण हुआ जिसे ज्यादा प्रखरता से भाजपा ने लड़ा लेकिन कांग्रेस का स्टैंड भी वहां वही था। लोगों ने देखा कि शायद भाजपा वाममोर्चा को नहीं हरा पाएगी इसलिए कांग्रेस को वोट दे दिया। वायनाड से राहुल के उम्मीदवार बनने के कारण वातावरण यह बना कि वे प्रधानमंत्री के लिए मतदान कर रहे हैं। जाहिर है, यह स्थायी स्थिति नहीं है। इन 23 सीटें में अत्यंत कम ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस की अपनी बदौलत जीती हुई स्वाभाविक माना जाए।
अगर द्रमुक से समझौता नहीं होता तथा केरल का वातावरण बदला नहीं होता तो कांग्रेस 2014 से भी बुरी स्थिति में पहुंचती। मत भी इतना इसलिए है, क्योंकि वह भाजपा के बाद सबसे ज्यादा 424 स्थानों पर लड़ी। 18 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में खाता न खुल पाना कांग्रेस के बारे में जनधारणा का स्पष्ट संकेत देने वाला है। जिन राज्यों में भाजपा से उसका सीधा सामना है वहां से वह 2014 के समान ही इस बार भी साफ हो गई।
छः महीना पहले राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में उसकी सरकार बनी थी। वहां की 51 में उसे 3 सीटें मिलीं। पंजाब में कैप्टन अमरींदर सिंह स्वायत्त रुप से काम कर रहे है। आतंकवाद, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, बालाकोट हवाई हमला आदि पर उनका रुख बिल्कुल भाजपा के समान है और उन्होंने वहां सम्मानजनक सीटें पार्टी को दिलवाई। कांग्रेस ने पिछली बार जीती 44 सीटों में से 2 सीटें सहयोगियों को दीं और 42 पर अपने उम्मीदवार उतारे। इनमें से 23 हार गए, केवल 19 जीते। इनमें 17 सीटों पर भाजपा ने तथा 3 पर इसके सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस से 3 सीटें छीनीं। इन सबकी चर्चा इसलिए जरुरी है ताकि यह आभास हो जाए कि भाजपा के सामने उसकी स्थिति क्या है।
अब प्रश्न है कि इसमें कांग्रेस के पास रास्ता क्या है? कांग्रेस का यह संकट आज का नहीं है। यह धीरे-धीरे बहुगुणित होते हुए 2014 और 2019 के परिणामों में केवल स्पष्ट हुआ है। किसे याद है सोनिया गांधी के नेतृत्व में 1999 के आम चुनाव में कांग्रेस ने तब तक के इतिहास में 114 सीटें तक गिर जाने का रिकॉर्ड बनाया था? 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार अवश्य बनी, लेकिन उसे केवल 145 सीटें ही मिलीं थीं और भाजपा को 138। वामदलों को 59 और अन्य कई दलों को सीटें मिल जाने के कारण भाजपा को बाहर रखने के नाम पर सरकार बन गई।
2004 में संघ परिवार के घटक ही भाजपा से नाराज थे और भाजपा के कार्यकर्ता निराश थे। उन्होंने काम ही नहीं किया था। इसलिए भाजपा की पराजय निश्चित थी। 2009 में भी लालकृष्ण आडवाणी को लेकर आकर्षण नहीं था। जिन्ना विवाद में वो अपनी आभा खो चुके थे तथा उन्होंने 2004 के बाद संघ परिवार के घटकों के साथ बैठकर उनको मनाने का कोई यत्न किया नहीं था। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक वर्ग मुलायम सिंह से नाराज था।
पश्चिम बंगाल में ममता के साथ तथा तमिलनाडु में द्रमुक के साथ गठबंधन, आंध्र में वाईएसआर की लोकप्रियता ने कांग्रेस को अप्रत्याशित 206 सीटें दिला दीं। यूपीए की सरकार बनी रही, इसलिए संकट की ओर ध्यान किसी का गया नहीं। जैसे ही नरेन्द्र मोदी के रुप में भाजपा का एक लोकप्रिय नेता सामने आ गया कांगेस वहां पहुंच गई जहां वह पहले ही पहुंच जाती। इसलिए यह कहना ही गलत है कि कांग्रेस का संकट आज का है।
कोई इस्तीफा दे दे उससे समस्या का हल नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि अगले दस दिनों में समीक्षा करके कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। यह सब समस्या को सही तरीके से नहीं समझ पाने का संकेत है। बिहार और उत्तर प्रदेश में दो तिहाई से ज्यादा प्रखंडों में उसकी ईकाई नहीं है। यह क्या आज की समस्या है?
पश्चिम बंगाल में उसका संगठन ध्वस्त हो चुका है। यह केवल इस चुनाव में तो नहीं हुआ। इसी तरह आंध्रप्रदेश और तेलांगना में कांग्रेस कहीं बची ही नहीं है। उड़ीसा में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र में कुछ नेताओें के क्षेत्रों को छोड़ दें तो जर्जर है। तमिलनाडु में उसका अस्तित्व द्रमुक पर टिका हुआ है।
पूर्वोत्तर में भाजपा एवं क्षेत्रीय दल उसका स्थानापन्न कर चुके है। जब इतने व्यापक क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन ही नहीं है तो फिर वोट लाएगा कौन? राजस्थान और मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय का सर्वप्रमुख कारण अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून में उच्चतम न्यायालय के संशोधन को निरस्त करना था। उसके खिलाफ एक वर्ग या तो कांग्रेस का वोट दे दिया या नोटा दबा दिया। इसे कांग्रेस ने अपने पक्ष में जनादेश समझने की भूल कर दी। मतों के हिसाब से देखें तो भाजपा और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं था। यह कभी पाटा जा सकता था। चुनाव परिणाम के बाद अपना मताधार बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने इन राज्यों में किया क्या? कुछ नहीं। चौकीदार चोर है के नारे से लोग आपको वोट देंगे यह कल्पना वही कर सकता था जिसे जमीनी यथार्थ का बिल्कुल पता नहीं।
वस्तुतः कांग्रेस लंबे समय से नीति, नेतृत्व और रणनीति को लेकर भ्रम का शिकार रही है। नीति का मतलब है विचारधारा। कांग्रेस की विचारधारा क्या है यही आज स्पष्ट नहीं है। इस बार का उसका घोषणा पत्र कई पहलुओं में अतिवादी वामपंथियों का घोषणा पत्र लगता था। यह देश में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली तथा स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत की पार्टी के वैचारिक दिशाभ्रम का प्रमाण ही है।
जब आपके पास विचारधारा नहीं है तो फिर आप समय के अनुसार मुद्दे उठाते हैं या आपसे जुड़े लोग प्रभावित कर आपसे अपना एजेंडा मुद्दे के रुप में उठवा देते हैं। यही कांग्रेस में पिछले डेढ़ दशक से हो रहा है। पार्टी ने थोक के भाव में पैनलिस्ट एवं प्रवक्ता बना दिए हैं जिनमें से ज्यादातर को पार्टी का इतिहास ही नहीं पता। वो असहमति का दुश्मनी मानकर टीवी चैनलों, एंकरों, पत्रकारों तक को अपमानित करते रहते हैं। कांग्रेस को ऐसा नेतृत्व नहीं मिला जिसमें लोग धीरता, गंभीरता, जिम्मेदारी, परिपक्ता, दूरदर्शिता, संतुलन और सम्पूर्ण समर्पण देख सकें। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को नेतृत्व हस्तांतरण किया गया, क्योंकि आज की कांग्रेस में यह विचार घनीभूत है कि उस नेहरु-इंदिरा परिवार से बाहर के व्यक्ति को यदि अध्यक्ष बनाया गया तो कांग्रेस एक नहीं रह सकती।
यह विचित्र विचार है। जब आप नेतृत्व एक ही परिवार तक सीमित कर देंगे तो फिर नीचे से उपर तक योग्यता और क्षमता कसौटी नही रह जाएगी। इसका परिणाम है, संकट का नीचे तक विस्तारित हो जाना। अगर अध्यक्ष बने तो साथ में एक थिंक टैंक का समूह होता जिसमें चुनकर लोगों को लाया जाता।
2014 की पराजय के बाद ए. के. एंटनी की अध्य़क्षता में बनी समिति ने एक रिपोर्ट दी थी। कायदे से उसे कांग्रेस कार्यसमित नहीं उससे बड़े समूह के बीच रखा जाना चाहिए था। कहा जाता है कि उसकी अनुशंसाओं को राहुल गांधी और उनके सलाहकारों ने अपने अनुसार अर्थ लगाया तथा कदम उठाए। युवा चेहरे को आगे किया तथा संतुलन बनाने के लिए कुछ अनुभवी लोगों को भी टीम मे शामिल कर लिया। इसमें वही लोग हैं जो हर बात में जी बोल सकते हैं। पार्टी में कार्यकर्ता बनने का चरित्र निःशेष है।
सेवा दल मृतप्राय है जिसमें कार्यकर्ता बनने का प्रशिक्षण मिल जाता था। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन दिल्ली या कुछ और जगहों तक सीमित हो गया है। इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जहां से कार्यकर्ता और नेता निकलने की संभावना ज्यादा होती है वह केवल नाम के लिए ही रह गया है। तो जहां से आपको नेता, कार्यकर्ता, विचार और फीडबैक मिलते थे वो सारे स्रोत सूख गए हैं। इसमें सही रणनीति बन ही नहीं सकती।
तो संकट बहुआयामी है जो पार्टी के व्यापक आंतरिक सुधार की मांग करती है। वर्तमान कांगेस से इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतनी दूर तक कोई सोचने वाला है ही नहीं। जो हैं वे हाशिए पर या बाहर हैं। उन सबको तलाश कर महत्वपूर्ण भूमिका में लाना, लंबे समय के लिए चुनावी प्रदर्शन की चिंता छोड़कर केवल संगठन को मजबूत करने के लिए अहर्निश परिश्रम करना और इसके साथ-साथ बिना एनजीओ, एक्टिविस्टों तथा कम्युनिस्टों से प्रभावित हुए जनता के मुद्दों पर संघर्ष करते हुए जनसमर्थन बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन वह एक अलग कांग्रेस होगी जिसमें आज के ज्यादातर चेहरे नहीं होगे। पार्टी पर कुंडली मारे लोग ऐसा होने नहीं देंगे।
अवधेश कुमार
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं)
Last Updated Jun 1, 2019, 2:55 PM IST